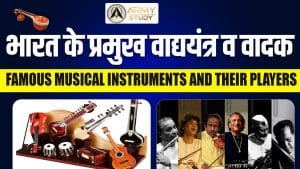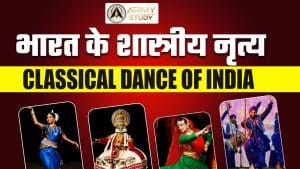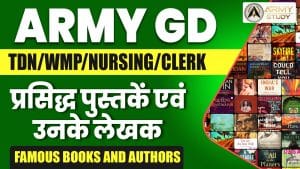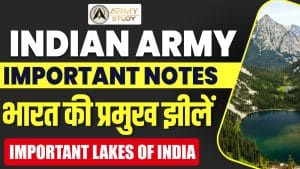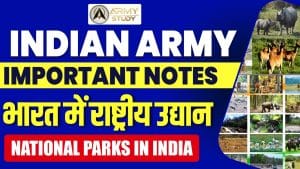Last updated on June 21st, 2025 at 01:40 pm
UNFPA जनसंख्या रिपोर्ट – 2025 भारत बना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश
UNFPA (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष) ने अपनी विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट (State of World Population – SOWP) 2025 “The Real Fertility Crisis” अर्थात् “वास्तविक प्रजनन संकट” शीर्षक से जारी की है। यह रिपोर्ट न केवल भारत को विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश घोषित करती है, बल्कि प्रजनन क्षमता, उम्र बढ़ने, और जनसांख्यिकीय चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है।
मुख्य बिंदु: भारत से जुड़ी प्रमुख बातें
जनसंख्या का आकार: अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ आँकी गई है।
भविष्य का अनुमान: 2060 के दशक की शुरुआत तक भारत की जनसंख्या 170 करोड़ तक पहुँच सकती है, इसके बाद इसमें धीरे-धीरे गिरावट की संभावना है।
जीवन प्रत्याशा: पुरुषों के लिए औसत 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष अनुमानित है।
प्रजनन दर (TFR): भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिरकर 1.9 हो चुकी है।
प्रजनन रुझान और क्षेत्रीय अंतर
SRS 2021 के अनुसार, भारत की TFR 2.0 रही – यह एक बड़ी उपलब्धि है।
उच्च TFR वाले राज्य:
- बिहार: 3.0
- मेघालय: 2.9
- उत्तर प्रदेश: 2.7
31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रतिस्थापन स्तर से नीचे हैं।
7 राज्यों में शहरी-ग्रामीण प्रजनन दर में अंतर बना हुआ है।
प्रजनन असमानता: बिहार, झारखंड, यूपी जैसे राज्यों में उच्च TFR और केरल, दिल्ली, तमिलनाडु में कम TFR देखा गया – यह शिक्षा, स्वास्थ्य, और लैंगिक भेदभाव पर आधारित असमानता को दर्शाता है।
प्रजनन स्वायत्तता में बाधाएँ
भारत में परिवार नियोजन निर्णयों को कई चुनौतियाँ प्रभावित करती हैं:
वित्तीय समस्याएँ – 40%
आवास की कमी – 22%
रोज़गार असुरक्षा – 21%
बाल देखभाल की सुविधा की कमी – 18%
बाँझपन – 13%
मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति – 14%
सामाजिक दबाव और जलवायु, राजनीतिक-अर्थव्यवस्था की चिंता – 19%
भारत की जनसंख्या संरचना और आँकड़े
| सूचक | मूल्य / अनुमान |
|---|---|
| भारत की औसत आयु | 28.2 वर्ष |
| कार्यशील आयु जनसंख्या (15-64) | 68% (लगभग 961 मिलियन) |
| 0-14 वर्ष की जनसंख्या | 24% |
| 10-24 वर्ष आयु वर्ग | 26% |
| वरिष्ठ नागरिक (65+) | 7% |
| पुरुष साक्षरता दर | 87.4% (NFHS-5) |
| महिला साक्षरता दर | 71.5% (NFHS-5) |
| कुल साक्षरता दर (15+ आयु वर्ग) | 77.7% (NSO 2021) |
| श्रम बल भागीदारी दर (पुरुष) | 78.8% |
| श्रम बल भागीदारी दर (महिला) | 41.7% |
| कुल LFPR | 60.1% |
| निर्भरता अनुपात | 47% (हर 100 कामकाजी लोगों पर 47 आश्रित) |
| जलवायु-संवेदनशील जनसंख्या | 80% से अधिक |
| NCD से ग्रस्त जनसंख्या | 20%+ |
| मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ | लगभग 15% |
नीति सुझाव: क्या होना चाहिए भारत का फोकस?
जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि प्रजनन अधिकारों को प्राथमिकता।
गर्भनिरोधक, मातृत्व देखभाल, बाँझपन और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की सभी के लिए पहुँच।
अविवाहित, LGBTQIA+, हाशिये पर रहने वाले समूहों को सेवाओं में शामिल करना।
सांस्कृतिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक पहल।
बाल देखभाल, आवास, और रोजगार जैसे ढांचागत मुद्दों को दूर करना।
UNFPA क्या है? – एक परिचय
UNFPA (United Nations Population Fund) संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सहायक संस्था है, जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए 150+ देशों में कार्य कर रही है। यह विश्व की लगभग 80% जनसंख्या को कवर करता है।
- स्थापना: 1969 में “संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष” के रूप में।
- नाम परिवर्तन: 1987 में “United Nations Population Fund”, पर संक्षिप्त नाम UNFPA ही रखा गया।
- लक्ष्य:
- हर गर्भावस्था वांछित हो
- हर प्रसव सुरक्षित हो
- हर युवा अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचे
- 2030 तक 3 परिवर्तनकारी लक्ष्य:
- परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकताओं को शून्य करना
- रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु दर को शून्य करना
- लैंगिक हिंसा, बाल विवाह व FGM जैसी हानिकारक प्रथाओं को शून्य करना
UNFPA सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) विशेषकर SDG 3 (स्वास्थ्य), SDG 4 (शिक्षा) और SDG 5 (लैंगिक समानता) का भी समर्थन करता है।
UNFPA की रिपोर्ट भारत को महज़ “सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश” नहीं बताती, बल्कि यह नीतिगत सुधार, लैंगिक समानता, युवाओं में निवेश, और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करती है। यदि भारत इन दिशा-निर्देशों का पालन करे, तो वह न केवल जनसंख्या की चुनौती को अवसर में बदल सकता है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में भी अग्रसर हो सकता है।